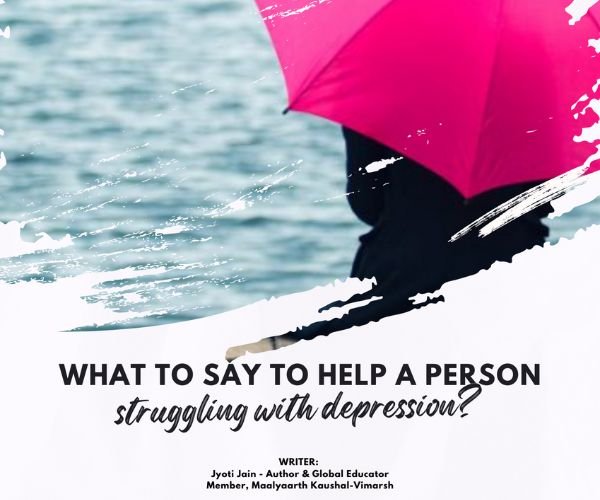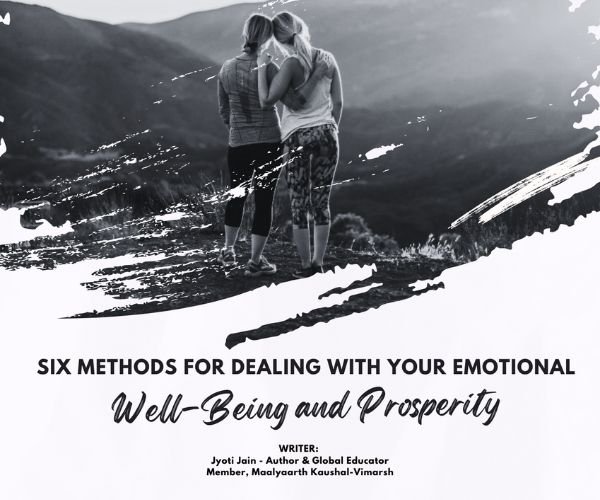- Have any questions?
- +91 9599935527
- maalyaarthfoundatioon@gmail.com
लोक एवं शास्त्रीय नृत्यों की पारस्परिकता लेखिका सुमीता शर्मा

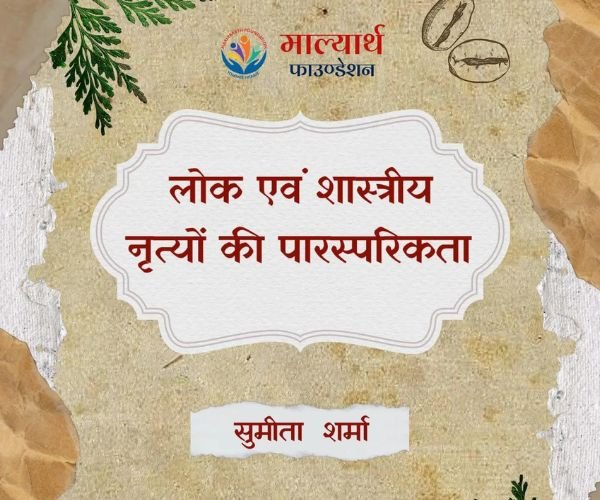
लोक एवं शास्त्रीय नृत्यों की पारस्परिकता
लोकनृत्य और शास्त्रीय नृत्यों की पारस्परिकता समझने के लिए साहित्य अनुशीलन करना एक रोचक एवं शिक्षाप्रद अनुभव देता है । हमारे आदिदेव शिव के अनेक नामों में से एक नाम है -अर्धनारीश्वर । हम सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरानुसार नृत्यकला का उद्भव आदिदेव शिव से हुआ है। 'अर्धनारीश्वर' भगवान शिव के नर्तन-स्वरूप को प्रतिष्ठित करता है जिसमें शिव जी ने अपने दाहिने पुरुष - भाग से " ताण्डव - नर्तन" की सृष्टि की है और बाँयें भाग या वाम अंग से “ लास्य- नर्तन" की सृष्टि की। इन दोनों भागों के सूक्ष्म जगत में परस्पर मिलन से ही सृष्टि को, सृजन को, शिव-स्वरूप को और नर्तन - कला को पूर्णता प्राप्त हुई ।
जैसा कि महाकवि कालिदास ने लिखा है :-
देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषंरुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गेविभक्तं द्विधा ।
त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते
नाट्य भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम् ॥
अर्थात् - मुनिजन कहते हैं कि यह नाट्य तो देवताओं की आँखों को सुहाने वाला यज्ञ है। स्वयं शिव जी ने उमा से विवाह करके अपने शरीर में ही इसके दो भाग कर दिए हैं - एक ताण्डव और दूसरा लास्य । इसमें सत्व, रज और तम तीनों गुण भी दिखाई पड़ते हैं और नाना रसों में लोगों के चरित्र भी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए अलग-अलग रूचि वाले लोगों के लिए प्रायः नाट्य ही एक ऐसा उत्सव है जिसमें सबको समान आनंद प्राप्त होता है ।
हमारी शास्त्रीय परंपरा में इसी ताण्डव को 'नृत्त' और लास्य को 'नृत्य' कहा गया है। जैसा कि नृत्त रत्नावली में जयप सेनानी ने लिखा है - " नृत्तं पुरुषकृतं ज्ञेयं नृत्यं नारीकृतं तथा ।” नृत्त पृरुषों द्वारा किया जाने वाला समझना चाहिए और नृत्य स्त्रियों द्वारा । नर्तन कला का जो कठोर या अधिक श्रम साध्य रूप है वही ताण्डव है, नृत्त है और जो इसकी अपेक्षाकृत अधिक सुकोमल व भाव प्रधान रूप है वही लास्य अर्थात् नृत्य है ।
आचार्य नन्दिकेश्वर ने कहा कि नृत्त भावाभिनय से रहित होता है - " भावाभिनय हीनं तु नृत्तमित्यभिधीयते ।” इस नृत्य का मुख्य आधार ताल व लय होता है - 'नृत्तं ताल्लयाश्रयम्।' आचार्य धनंजय कहते हैं जब ताल्लय के साथ भाव विहीन किन्तु सौंदर्यपूर्ण अंग-संचालन किया जाए तो उसे 'नृत्त' कहते हैं। यह नृत्त मानवीय उल्लास की चरम अभिव्यक्ति है और समस्त कलारूपों में सर्वप्रथम प्रस्फुटित हुआ है। - अभिनय दर्पण - आचार्य नंदिकेश्वर
प्रकृति और पुरुष की एकात्मता का नाम ही शिव हैं। शिव अंगों से उत्पन्न ताण्डव व लास्य भारत के ही नहीं वरन् संपूर्ण विश्व के नृत्यों की जननी है। लोकनृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों का ही उद्गम इस ताण्डव और लास्य की उत्पत्ति में है । प्रकृति प्रदत्त पुरूष प्रधान नृत्य को ताण्डव की संज्ञा दी गई है स्त्री प्रधान नृत्यों को लास्य की । इन प्राकृतिक एवं मानवीय प्रवृत्तियों का प्रथम प्रस्फुटन लोकनृत्यों में ही होता है और उन्हीं लोकनृत्यों को जब आचार्यवृंद एक व्यवस्था में ढाल देते हैं तो वे शास्त्रीय नृत्य कहलाने लगते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पुरुष प्रधान नृत्य केवल पुरुष ही करें। यह जरूरी नहीं कि स्त्री प्रधान नृत्य केवल स्त्रियाँ ही करें। लोकनृत्य में यह परंपरा रही है कि पुरुष ही स्त्री वेश धारण कर शिवप्रदत्त लास्य को अभिमंचित करते रहे हैं। अब ताण्डव अर्थात् पुरुष प्रधान नृत्यों में भी स्त्रियों का प्रवेश हो चुका है। लोक से निकलकर यह धारा शास्त्रीयता में पहुंची है। यदि राजस्थान के नृत्यों का संदर्भ लें तो लोक में नाचे जाने वाले गींदड़, धमाल, चंग, भवाई आदि में पदसंचालन प्रधान नृत्यों का सृजन हुआ, उन्हीं की प्रेरणा से कालांतर में कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ। इस शास्त्रीयता का यह परिणाम है कि कथक नृत्य केवल ताण्डव ही नहीं लास्य को भी अपने भीतर समाहित करता है यथा घूमर ।
देवता मूर्ति प्रकरणम् में सूत्रधार श्रीमंडन ने आठवें अध्याय के अंत में तीन श्लोकों में नृत्य के महत्व को प्रतिपादित हुए लिखा है
भंगे - भंगे मुखं कुर्याद्धस्तो दृष्टिं च नर्तने ।हस्तकाद्यं भवैल्लोके कर्मणोऽभिनयेऽखिलम् ॥ 22 ॥
नृत्य करते समय जिस प्रकार पैर विभिन्न रूप से चलित किया जाता है, उसी प्रकार मुँह व दोनों भुजाओं व दृष्टि को भी बनाया जाना चाहिए। (लोकांचल में हाथ, मुख और दृष्टि का अभिनय की दृष्टि से महत्व है । यथा - हस्तमुद्रा, मुखाभिनय व नयनमुद्रा ) ।
यतो हस्तस्ततो दृष्टिर्यतो दृष्टिस्ततो मनः।यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः || 23 ||
जिस प्रकार हाथ किसी विषय को बताता है, वैसे ही दृष्टि भी उसी विषय को स्पष्ट करती है। इसी प्रकार जैसी दृष्टि वैसा मन, जैसा मन, वैसा ही भाव, जैसा भाव वैसा ही रस प्रतीत होता है।
आस्येनाऽऽलम्बयेद् गीतं हस्तेनार्थ प्रकल्पयेत्।चक्षुम्यां च भवेद् भाव: पादाभ्यां ताल निर्णयः ॥24 ॥
मुख से गीत का निर्णय होता है । हाथ से अर्थ भाव की कल्पना होती है । दृष्टि से भाव की कल्पना होती है और पैर से ताल का निर्णय होता है । " निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस तथ्य से लोकनृत्यों के संबंध में हमारी संकुचित भावना का परिष्कार ही नहीं होता अपितु समझ का विस्तार होकर एक व्यापक रूप भी फलित होता है।”
नृत्य जब सहज संकेतों की भाषा में अपनी बात कहता है तब उसका दर्शक पर एक विशेष प्रभाव होता है। लेकिन शास्त्रीय आचार्य जब उन लोक संकेतों को विभिन्न भाविभिव्यक्तियों से जोड़ देते हैं तब नृत्य में एक नया निखार आ जाता है। राजस्थान में एक समय था ( कुछ मात्रा में आज भी ) जब स्त्रियाँ घूंघट निकाल कर नृत्य करती थीं इसलिए वहां लास्य की वह भावाभिव्यक्ति जो नृत्य संचालन से या मुख मुद्रा के माध्यम से व्यक्त की जाती है इसकी संभावना ही नहीं थी लेकिन धीरे-धीरे शास्त्रीयता के प्रभाव से मुखाकृति से भावाभिव्यक्ति करने वाली रचनाओं का निर्माण हुआ । वे रचनाएं अब केवल स्त्रियों द्वारा ही अभिमंचित नहीं होती वरन् पुरुष भी उस लास्य भावों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में अपने अंग-प्रत्यंग के माध्यम से व्यक्त करते हैं तथा अब शास्त्रीयता के साथ जुड़ कर स्त्रियों ने भी अपना घूंघट उठा दिया ।
उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण इस बात का द्योतक है कि लोक व शास्त्रीय नृत्य न तो परस्पर विरोधी हैं तथा न ही स्पर्धी । इनकी पारस्परिकता ने मानव की नृत्य विधा को संवारा है। शास्त्रीयता का अहंकार रख कर हमें लोक परम्परा में समाहित नृत्य प्रकारों को हेय नहीं मानना चाहिये वरन् कुछ उनसे सीखना चाहिये तथा उन्हें शास्त्रीयता का अधिष्ठान देना चाहिये । जब हम नृत्य साधना करते हैं, तब क्रमशः शिव हमारे शरीर में अवतरित होने लगते हैं। नृत्य एक पवित्र विधा है ।
विदुषी सुमीता शर्मासुविख्यात कथक नृत्यांगना
जयपुर घराना