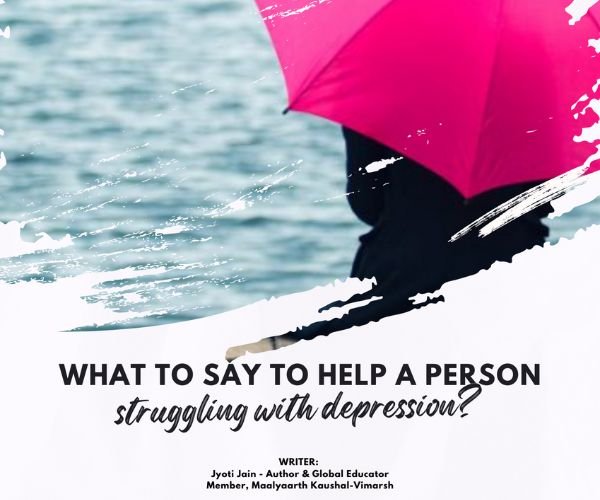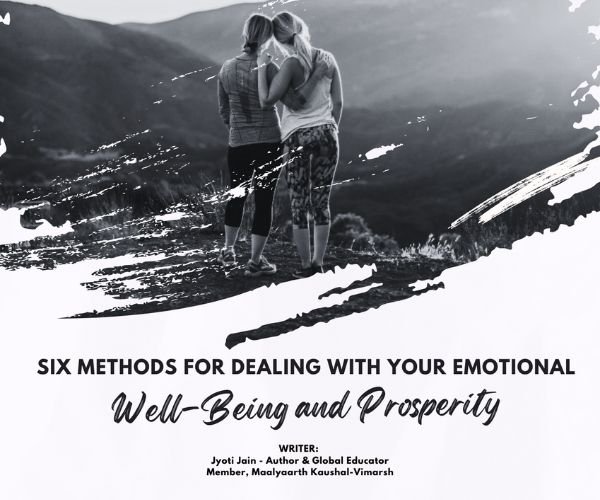- Have any questions?
- +91 9599935527
- maalyaarthfoundatioon@gmail.com
हरियाणा के लोकनाट्य और संस्कृति लेखक

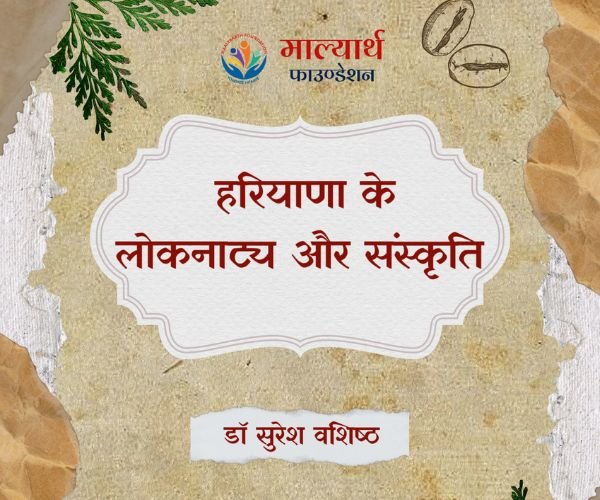
हरियाणा के लोकनाट्य और संस्कृति
हरियाणवी संस्कृति लोकलुभावन और भाईचारे की संस्कृति है। आपसी प्रेम और सौहार्द्र की सांझी विरासत है। यहाँ की लोकपरंपराओं में लोकहित सर्वोपरि रहा है। पंचायत में लिए गए निर्णय नियम बन जाते हैं और सभी उसका पालन भी करते है। यहाँ के लोक साहित्य में धार्मिक जीवन का चित्रण व्यापक रूप से प्रस्तुत हुआ है। अपने प्रत्येक कार्य की शुरुआत में यहाँ के लोग अपने इष्टदेव को याद करना नहीं भूलते । आदर भाव यहाँ का मूल मंत्र है।
कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गीता के उपदेश को दोहराया गया। विश्व को निष्काम कर्म करते रहना और भूत, वर्तमान एवं भविष्य के प्रति उसका मार्गदर्शन कराने वाला यह पवित्र ग्रंथ ‘श्रीमद्भागवत गीता’ इसी भूमि पर उच्चरित हुआ। द्रोणाचार्य द्वारा कुरुवंश के राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा भी इसी प्रांत के ‘गुरुग्राम’ में हुई। सुगठित और लोकहित निर्णय यहाँ के सदाचार हैं। इन्ही कारणों से इस प्रदेश को ‘देवभूमि’ भी कहा गया है। लोक आदर्श के लिए चिरसंचित अनुभव यहाँ की पहचान हैं। अपने प्रदर्शन रूप में यहाँ की संस्कृति जीवन के समस्त अनुभव को आत्मसात किए हुए है। ग्राम व्यवस्था सुदृढ़ और धर्म परायण है। गाँव की बैठकों, चौपालों या चबूतरों पर बैठकर यहाँ के लोग लोकहित और लोक आदर्श को आधार बनाते हैं और अपने निर्णय स्वयं कर लेते हैं।
हरियाणवी लोकमंच तटस्थ एवं प्रभावशाली है। लोकनाट्यों का अपना विशिष्ट स्थान है। लोकनाट्यों में मुख्यतः रासलीला, कृष्ण लीला, रामलीला, नौटंकी, भांड और सांग प्रसिद्ध नाट्य है। रामलीला को इस प्रदेश में अद्भुत लोकप्रियता हासिल है। दशहरे से पूर्व गाँव-गाँव में रामलीला का मंचन यहाँ की परंपरा में सम्मिलित है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक महानाट्य है। स्थानीय कलाकारों द्वारा जिसे बडे़ चाव व आदर से गाँव-गाँव में अभिनीत किया जाता है, राम वनगमन से रावण दहन तक इसे प्रस्तुत किया जाता रहा है। दृश्य योजना आडम्बर रहित रहती है। कथा मंडली-ढोलक, वाद्य या समवेत गायन द्वारा कथा को अभिनय के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। बीच-बीच में इनाम-इकराम भी चलता है। यहाँ के लोगों की भावनाएँ रामचरित के साथ जुड़ी हुई हैं, इसी से पूर्ण तन्मय होकर वे इस कथा का आनंद लेते हैं। इसमें पात्रों की वेशभूषा,रंगभूषा और रंगसज्जा में विशेष परिश्रम नहीं किया जाता वरन् कथा का महत्त्व अधिक रहता है। चंदन, खड़िया, रोली, मुकुट और गेरुआ वस्त्र के साथ धनुष-बाण आदि सामग्री ही पर्याप्त होती है।
ब्रजक्षेत्र की संस्कृति अपनी खास पहचान रखती है। वहाँ पर कृष्णलीला व रासलीला का महत्त्व अधिक है। नौटंकी का प्रदर्शन भी वहाँ बहुत होता है। रासलीला का स्थान अग्रणी है। यह महानाट्य खुले मंच पर अभिनीत होना वाला प्राण-नृत्य है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण संग श्री राधा और बहुत से गोप-गोपियाँ भी नृत्य करते है। नृत्य अभिनय के खास नियम होते हैं। बहुत सारे कृष्ण और राधा बहुतेरी रास रचाते हैं। रासलीला हरियाणा के ब्रजक्षेत्र का दर्पण है। भगवान रास रूप में प्रस्तुत होते हैं, इसी में उन्हें आनंद प्राप्त होता है। लीला-रस सृजन का माध्यम है।
रासलीला में कृष्ण कथा को एक नृत्य संगीतात्मक छवि प्रदान की गई है। कष्ण जीवन के विभिन्न प्रसंग, गोप-गोपिकाओ एवं अहीरों के विभिन्न प्रहसन इत्यादि इस लीला के बिन्दु है। साधारण मंचं, मंदिर या चबूतरे या ऊँचे तख्त डालकर मंच तैयार किया जाता है। रंगभूमि में गायक और वादक बैठते हैं और सरल, सहज अभिनय एवं संगीत की द्रुपद शैली दर्शकों को आत्मविभोर कर देती है। पर्दा उठने पर राधा-कृष्ण की युगल छवि की आरती की जाती है। तत्पश्चात लीला आरंभ होती है। कृष्ण का राधा संग, गोपियों-सखियों संग अनुरागपूर्ण वृत्ताकार नृत्य होता है। कृष्ण कभी गोपियों संग, तो कभी गोपियों से घिरकर नाचते हैं।
इसी क्षेत्र में नौटंकी या स्वांग का प्रचलन भी है। प्रायः विवाह आदि के सुअवसरों पर या होली के आसपास रसिया भाव संग इन्हें खेला जाता है। भेष बदलकर कला साधक स्वांग रचते हैं। ढोलक तथा नगाड़े इन नाट्यों के प्रिय वाद्य होते हैं। नौटंकी में ख्याल और स्वांग प्रदर्शित होते हैं। गीत, संगीत, नृत्य अभिनय एवं वाद्य आदि की दृष्टि से कथा गीत के माध्यम से स्वांग रचे जाते हैं और उन्हें नौटंकी शैली में अभिनीत किया जाता है। दर्शक और कलाकार प्रदर्शन के दौरान तन्मयता और एकसूत्रता बनाये रखते हैं। कोई विशेष मंच इसके लिए नहीं होता। मंच पर उपस्थित होकर अपने स्वरूप, भाव-भंगिमा को दर्शाते हुए भरसक मनोरंजन के साथ कथा को आगे बढाते हैं। कथा-किसी घटना की उपस्थिति भी हो सकती है।
खोडिया स्वांग भी संपूर्ण हरियाणा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। लोकशैली इसका प्राण है। यह स्त्रियो द्वारा अभिनीत होता है। ब्रज की माधुर्य मोहक शैली का प्रभाव इसमें रहता है। रोहतक, भिवानी, पानीपत, जींद, कैथल आदि में स्त्रियाँ बड़े चाव से इसे खेलती हैं। दुल्हा जब दुल्हन को बारात लेकर लिवाने जाता है, उसके बाद घर में स्त्रियाँ इस नाटय को खेलती हैं। स्त्रियाँ ही पुरुष वेश धारण करती हैं और हँसी-ठिठौली खूब होती हैं। गीत-गानांे की भी भरमार रहती है और चुटीले प्रसंग चलते हैं। इस खेल में पुरुषों का आना वर्जित रहता है।
स्वांग का तद ्भव रूप ही शुरू में ‘सांग’ रहा। बाद में यह खेल हरियाणा का प्रसिद्ध लोकनाट्य साबित हुआ। किशनलाल भाट से इसकी शुरुआत हुई। किशनलाल और उसके साथी रामायण की चैपाईयाँ गाते और जनाना वेशधारी उन्हें दोहराता हुआ नाचता। ढपली की थाप पर लोगों का मनोरंजन करता। भाट के बाद अमीचंद बंजारा और उसका भाई सामने आए और बेडा तैयार किया। ढपली की जगह ढोलक का इस्तेमाल हुआ। आगे चलकर पं. दीपचंद शमिल हुए। दीपचंद ने इस नाट्य को महानाट्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन्होंने चार लड़कों को जनाना वेश दिया और एक नकलची खड़ा किया।
पं. दीपचंद यहीं के निवासी थे और यहाँ की भाषा और संस्कृति से भली-भाँति परिचित थे। उन्होंने ‘सांग’ को नए रूप में खड़ा किया। गीत और संगीत को विकसित किया। अर्थात् साधु-संतों और भक्तों, शादी-ब्याह के रसीले गीतों, डोमनियों और हरकारों के किस्सों, भजन प्रवृत्ति में लिप्त संस्कारभाव, भक्ति-श्रद्वा और वीरता से लिप्त कथाओं को आधार मानकर सांग का रूप विकसित हुआ। इस परंपरा में अनेक स्तंभ बने। पं. दीपचंद के शिष्य हुए पं. हरदेव स्वामी और उनके शिष्य हुए बाजे भगत। उसी दौरान बाबा मुआसीनाथ के शिष्यत्व में भजनी मानसिंह और उनके शिष्य पं. लख्मीचंद का आर्विभाव हुआ। इन्ही सबों के अथक प्रयास में पश्चिमी हरियाणा का यह नाट्य काफी लोकप्रिय हुआ। संघियों द्वारा रचे गए कथ्य, रागनियों के द्वारा गाँव-गाँव में गाए जाते हैं, निहाल दे, नल-दम्यंति, जानी-चोर, रूप कंवर, ढोल कंवर, नौटंकी कथा आदि पौराणिक किस्से आज भी लोगों का भरपूर मनोरंजन करते हैं।
सांग मंडली में पंद्रह-बीस के आस-पास कलाकार होते हैं। कुछ जनाना वेष धारण कर नृत्य दिखाते हैं, कुछ संगीत-वाद्य बजाते हैं और मुखिया मर्दाना वेश में रागनियों द्वारा कथा के सूत्र खोलता हुआ आगे बढ़ाता रहता है। बाकी सभी प्रस्तुत कथा को एक रूप और एक स्वर देते हुए गाते हैं, एक बड़े मैदान में तीन-चार तख्त डालकर मंच तैयार किया जाता है। बीच में साजिंदे बैठते हैं। हुक्का भी रखा होता है। चारों किनारों पर जनाना वेशधारी नाचते हैं। कथा के सूत्र खोलता हुआ मुखिया आगे बढ़ता है, चारों वेशधारी गाते हुए कोने बदलते रहते हैं। साजिन्दे भी साथ में गाते हैं। बीच-बीच में नकलची व्यंग्य कसता है और लोगों को हँसाता है।
हरियाणा प्रदेश का जानोल्लास ‘सांग’ के द्वारा प्रस्फुटित होता है। कथागीत इसका प्राण है और यह नाटकीय रूप में चलता है। चैबोल, त्रिबोल, दोहा, तोड़ और रागिनी का एक-एक शब्द श्रृंगार और वीररस के ताने-बाने से बुना होता है। श्रोताओं में यह महानाट्य अपनी अमिट छाप छोड़ता है। सांगी का अरररर........का खींचा स्वर जादू-सा असर करता है।
हरियाणवी लोग अपनी नीरवता को मिटाने के लिए बहुत से ढंग अपनाते हैं। अखाडे़ में कुश्ती, कब्बड़ी, रागनियों की स्वर तान छेड़ देना इत्यादि। स्त्रियाँ भी गीत गाकर, नाचकर अपना मन बहलाती हैं। कथाएँ और रोचक पहेलियाँ सुनना-सुनाना भी यहाँ के लोगों का शौक है। कभी-कभार लोककवि भी गाँव में आकर अपने गायन से मन मोह लेते हैं। नट-नटी भी अपनी कला से करतब दिखलाते हैं। सावन का झूला झूलते-झुलाते हुए गीतों की बहार भी रहती है। स्त्रियाँ सावन माह में अपने भाई की प्रतीक्षा में गाती हैं। प्रियतम की याद के गीत भी यहाँ प्रचलित हैं। गाते-बजाते सब एक-दूसरे की बलैयॅा लेती हैं, ढोलक की थाप पर थिरक जाना और उल्लास प्रकट करना यहाँ का हुनर है। स्त्रियाँ व्रत-त्यौहारों पर रतजगा करती हैं और हँसी-ठिठौली में आनंदमग्न रहती हैं। यहाँ के लोकगीतों में संपूर्ण हरियाणवी लोक-जीवन की छवि बड़ी सुंदर और कलात्मक ढंग में प्रस्तुत होती है और होती रहेगी।
डाॅ सुरेश वशिष्ठ
प्रांत उपाध्यक्ष
संस्कार भारती हरियाणा