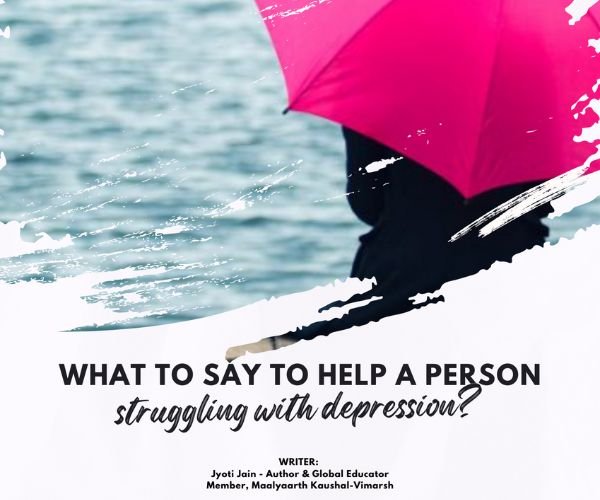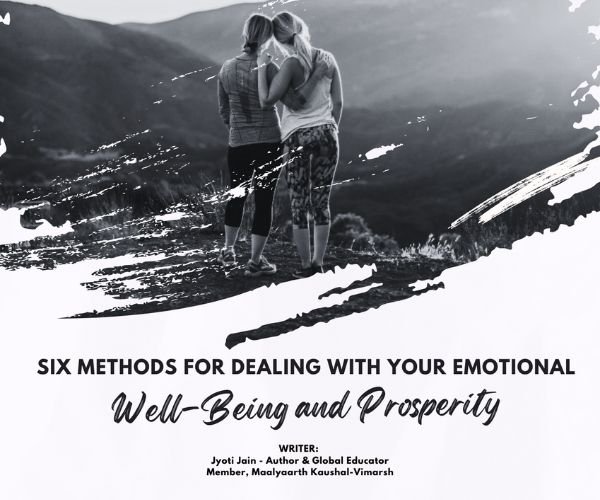- Have any questions?
- +91 9599935527
- maalyaarthfoundatioon@gmail.com
कला से जुड़ाव और प्रभाव

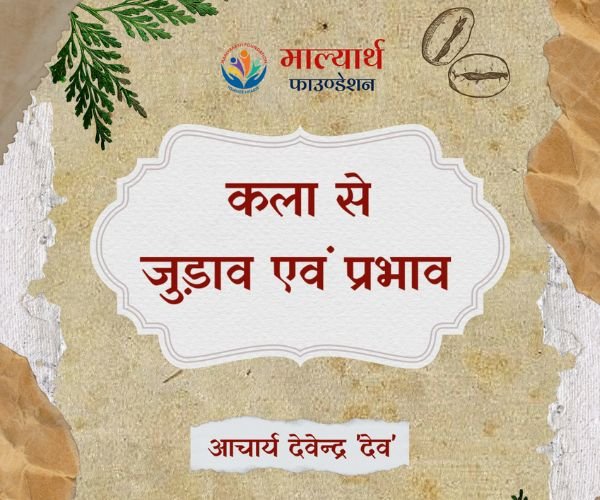
कला से जुड़ाव और प्रभाव
जीवन पूर्वजन्मों के कर्मों के परिणामस्वरुप ईश्वर द्वारा प्रदत्त वह समयावधि है जिसमें व्यक्ति को अपनी पिछली भूलें सुधारने और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण करने का भरपूर अवसर मिलता है किंतु दुर्भाग्य से मनुष्य उसके महत्व को नहीं समझता और उसे यूं ही गुजार देता है।मुमूर्छा (कोमा) में पड़े व्यक्ति के समान केवल सांसों की गिनती पूरी करने अथवा केंचुए के समान केवल भोजन और उत्सृजन करने का भी नाम जीवन नहीं है।यदि मानव वास्तव में इस कालावधि का उचित उपयोग करना चाहे तो कला, चाहे वह किसी प्रकार की हो, उसकी पर्याप्त सहायता कर सकती है। कवि के शब्दों में-
जीवन पाना बहुत सरल पर जीवन जीना एक कला है।सुविधाओं की कल्प-लोक ने वर्तमान को सदा छला है।
भटक रहे सब अपने-अपने नए सुखों की आशाओं में।
तृप्ति भला कैसे मिल पाए उलझन है परिभाषाओं में।
सब झूठे आश्वासन देकर खुद को बहलाते रहते हैं।
उनको देखो जो दुख पाने पर भी मुस्सकाते रहते हैं।
'कला' शब्द 'क' और 'ला' इन दो व्यंजनों से मिलकर बना है।'क' से तात्पर्य 'कलय' अर्थात रंजन अर्थात रँगना और 'ला' से तात्पर्य दास्य अर्थात नृत्य की मनमोहक भाव-मुद्रा। कलय का प्रचलित भावार्थ है कलई करना अर्थात रंगना। किससे रँगना, मनभावन रंगों से। मनभावन रंगों वाली कलाएं चौसठ प्रकार की होती हैं जिनमें कुछ मन,प्राण और अंतरात्मा को रंगने का काम करती हें तो कुछ जीविका जीविकोपार्जन के काम आती हे।गीत संगीत नाट्य नृत्य, लोककला, चित्रकला भूअलंकरण आदि कलाएं ऐसी है जो न केवल व्यक्ति के अंतर्मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हे प्रत्युत् निकटवर्ती समाज व परिवेश को भी अच्छे से प्रभावित करती हे।ये कलाएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुषुप्त बीज की रुप में विद्यमान रहती हे जिन्हें दुलारकर पुचकार कर जगाया पोसा धोया पोछा सजाया और संविरा जा सकता है।जो व्यक्ति कला से स्वयं को सर्वथा असम्पृक्त असम्बद्ध अपरिचित बताते हैं अथवा उदासीन बनते हे, वे या तू महाअज्ञानी हे या अलीकवादी (झूठे) हैं।कहा जाता है कि रोना गाना इस दुनिया में सब को आता है, यहां तक कि जिन्हें हम जड़ समझते हैं उन्हें भी।यह अलग बात है कि मानवेतर प्राणियों पदार्थों के रोने गाने की भाषा हम न समझते हों। अशरफुलमखलूकात कहलाने वाले मनुष्यों में कोई स्टेजसिंगर,कोई स्ट्रीट सिंगर तो कोई बाथरूम सिंगर।
साहित्यसंगीतकलाविहीना:साक्षात पशुपुच्छ विषाचहीना:
अर्थात जो साहित्, संगीत कला से विहीन हैं वे विदा सींग,पूंछ के साक्षात पशु के समान हैं। आज के युग में जब संगीत विद्या तंत्र प्रणाली (म्यूजिकल थेरैपी) से दुधारु पशु भी अधिक दूध देने लगे हैं, विशेष प्रकार की आवाजें निकाल कर पशु एकत्र किये जा रहे हैं तो ऐसे में क्या यह तथाकथित मनुष्य अपने को पशुओं से भी गया बीता सिद्ध करना चाहते हैं।संगीत से अनिद्रा जैसे असाध्य रोगों का उपचार हो रहा हे योगशालाएं चल रही हे और भी न जाने कितने प्रकार से प्रयोग किये जा रहे कला के क्षेत्र में। ये सारे दृष्टांत यह सिद्ध के लिए पर्याप्त हैं कि कला से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपने मन को और मन के माध्यम से अपने तन को न केवल स्वस्थ कर सकता हे अपितु शक्तिशाली भी बना सकता है।
शैशव में जब हमारी बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ था, प्रभातियां सुनकर हम जागते थे,माँ की लोरियां सुनकर हम बहलते थे, हमें नींद भी आती थी।कुछ और बड़े हुए तो डुगडुगी, बासुरी पींपनी सीटी हमारे मन बहलाने के साधन बने। छात्र जीवन में लगातार तीन-साढ़े तीन घंटे पढ़ाई में मगज खपाने के बाद इंटरवल की घंटी सुनकर किलकार भरते हुए हमसे कक्षा से बाहर आते थे।वह उस समय की कविता थी, मन का संगीत था।आज ऐसा भला कौन हो सकता हे जिसका जीवन बहुआयामी गीत संगीत कला के इन देहरी-द्वारों से होकर न गुजरा हो। भौतिक आपाधापी में अपने को फाँसकर, रसात्मखता से विरक्ति पालकर कला से ही नहीं हम अपने जीवन से भी दूर होते जा रहे हैं। हमारी सांसे बोझिल होती जा रही हे।इंद्रियां असमय ही शिथिल हो रही हे।हम समय से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं।यह हमारी मजबूरी कम मारूरी अधिक है।यह सायास ओढ़ी हुई व्यस्तता हमें अस्तता की ओर ले जा रही है।इन स्थितियों को अब भी रोका जा सकता हे, रोकना ही होगा। संवेदनाएं जाग्रत करके, कला व कलाकार के साथ अपने को जोड़कर।
माल्यार्थ फाउंडेशन कला,साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली अखिल भारतीय संस्था है जो बिना किसी लाभ-लोभ की भावना के गीत, संगीत,नाट्य, नृत्य, लोककला चित्रकला भूअलंकरण आदि नौ विधाओं में कार्य कर रही है।उसका विधा परिवार तीन रूपों में रहता है-
- कलाकार/कलासाधक
- कलारसिक/ कलावधानी और
- दोनों के मध्य योजक जिसे हम व्यवस्थापक या आयोजक भी कह सकते हैं।
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इन तीनों में से किसी एक वर्ग में न आता हो। हम अनुभव कर सकते हे कि बाल्यावस्था में हमारे पारिवारिक उत्सव ऐसे ही आयोजनों के केन्द्र होते थे, वहां ऐसी ही समन्वित कला प्रस्तुतियां होती थीं, जिनका स्थान आज पाश्चात्य प्रणालियों ने ले लिया है। पहले विद्यार्थी जीवन में साप्ताहिक संगोष्ठियां होती थी जिनमें गीत संगीत जैसी कला के प्रति अभिरुचि जगाने, उन्हें प्रस्तुत कराने के प्रयास कक्षाध्यापकों गुरुजनों द्वारा किये जाते थे।विविध राष्ट्रीय अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटक फैंसी ड्रेस वाद-विवाद प्रतियोगिता कवि दरबाथ होते थे जिनमें विद्यार्थी बढ़-चढ़कर भाग लेते थे।
आज हम व्यस्त नहीं महा व्यस्त हैं। हमारे पास अपने लिए समय नहीं है।हम या तो नौकरी करते हैं,व्यापार करते हैं, खेती करते हैं या किसी की मजदूरी।कार्यालय में लगातार कार्य करते करते थक जाते हैं तो या तो तंबाकू मलने लगते हैं ,धूम्रपान करते हैं या गुटखा का सेवन करके थकान दूर करते हैं अथवा शाम को मदिरा का सहारा लेते हैं। यह सब केवल शरीर के लिए ही नहीं,अपने जीवन के लिए और आने वाली संतति के लिए भी महाघातक हे जिसके बारे में हम सोचते नहीं, फिर रोते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते।पीढ़ी बर्बाद हो रही है।अरे, क्यों नहीं होगी? आपने थकान दूर करने के नाम पर कितने सुंदर विकल्प तलाश रखें हैं? अरे भाई, ऐसे भी यदि हम अपने पुराने किसी प्रिय गीत की एक कड़ी मुक्तकंठ से गा लें, गुनगुना लें तो न केवल थकान अधिक अच्छे से दूर हो सकती है, नई चेतना भी जाग्रत हो सकती है।उसकी तरंगों में इतनी शक्ति होती है।
किसान सुबह से खेत जोत कर जब दोपहरी को पेड़ की छांव में सुस्ताने आता है तो किसी लोकगीत की धुन छेड़ बैठता हे जो न केवल उसकी सारी धकान दूर कर देती है प्रत्युत अगले कार्य के लिए उसे उसे स्फूर्त, तरोजाजा भी कर देती है।व्यापारी संगीत सुनकर थकान दूर कर सकता है।मजदूर तो प्राय: रंगाई-पुताई ठोंका पीटी करते समय ईट पत्थर ढोते समय मोबाइल पर ही गीत संगीत सुनते रहते हैं।योग कक्षाएं संगीत की मचलती धुन पर चलती हैं।घरों में महिलाएं खाना पकाते समय या अन्य कोई घरेलू कार्य करते समय गीत गाती रहती है।यहां तक कि काम वाली बाइयां भी गले में मोबाइल लटकाकर इसी ढंग से झाड़ू पोछे का, बर्तन कपड़ा धोने जैसे घरेलू काम निपटाती हैं। महीने वो महीने, चार-छ: महीने में या वर्ष में एक बार जब कभी परिवार के साथ हम भ्रमण या पर्यटन पर जाते हैं तो नदियों,समुद्रों के तटों पर लहरों का, पक्षियों के कलरवों का, पशुओं की भंगिमाओं का,झरनों का हवाओं का संगीत सुनने ही तो जाते हैं।आकाश ने काले भूरे बादलों की इन्द्रधनुषी छटाओं की मनोरम चित्रकारी का आनंद लेने, खेतों की लहराती फसलों की झूम झटक,उन का नर्तन,पर्वत मालाओं का विशुभ्र हिमानी का हास-परिहास ही तो देखने जाते हैं और यह सब देख कर साल भर के लिए तरोताजा होकर लौटते हैं।
हम यह भी जान लें कि यह कला ईश-प्रदत्त एक विशेष उपहार होती हे।यदी हम इसका उपयोग सम्मान नहीं करते तो सामाजिक पातक के साथ-साथ आध्यात्मिक अपराध भी कारित करते हैं जिसका परिणाम गूलर के फूल की भांति कभी भी किसी भी रुप गए हमें भोगना पड़ सकता है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
मैने खेतों में,कल-कारखानों में,कार्यालयों में विलक्षण प्रतिभाओं से संपन्न मजदूरों, कर्मचारियों को विशेष अवसरों पर कला-प्रस्तुतियों के पारितोषिक स्वरुप,उन्हीं के कलारसिक भू-स्वामियों,उद्योगपतियों और अधिकारियों द्वारा सम्मानित होते देखा है। वे सम्मान देते लेते समय दोनों की आंखों में विशेष प्रकार की अवर्णनीय चमक मैंने देखी है।
हम सुबह शाम पूजन के साथ भजन आरती की औपचारिकता निभाते ही हैं।क्यों न हम स्थाई रुप से इसे अपने जीवन का अंग बना लें।इन कलाओं को अपने अंदर जागृत और विकसित करके और यथावसर सार्वजनिकरूप से उसे प्रस्तुत कर के उसी ईश्वर की समाराधना करें जिसने यह सब हमें दिया हे। क्यों न सामूहिकरुप से मिल बैठकर उस चरम परम सत्ता का, इस समाज का ऋण चुकाएं औरों को प्रसन्न करके, उनका सम्मान प्राप्त करके स्वयं का जीवन धन्य करें।बाल्यावस्था में देखे गए सत्य हरिश्चंद्र और श्रवणकुमार के नाटकों ने गांधीजी का जीवन बदल दिया।योगिराज कृष्ण के विश्व विराट रुप ने मोहान्ध अर्जुन को कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए प्रवृत्त कर दिया था।चंद वरदई के शब्द संकेतों में अंधे पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी का वध करा दिया था। ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं।
कला-साहित्य से जुड़कर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता?उसकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यूँ डूबने के हजार तरीके हैं परन्तु उबरने का एक ही रास्ता है और वह है उपयुक्त व्यवस्थानुनुसार कला से जुड़कर अपने को सँवारना।
जीने की तमन्ना हे तो बिखरा दो फ़र्क परपत्थर भी तुम्हें देखकर परवाज सीख ले
मरना हो अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो
दुनिया तुम्हीं से मरने का अंदाज सीख ले।
यदि हम ऐसा कर सके तो स्वर्गिक सुख की गंगा को धरती पर उतार कर लाने वाले, नव युग के भागीरथों में सहज रुप से हम अपनी भी गणना करा सकेंगे।जय भारत जय भारती।
- आचार्य देवेन्द्र 'देव'
वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार